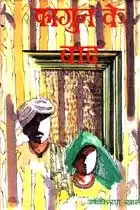|
सामाजिक >> फागुन के बाद फागुन के बादउषाकिरण खान
|
406 पाठक हैं |
||||||
बिहार के ग्रामीण परिवेश पर लिखा गया नितांत अनूठा उपन्यास...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘‘क्या हुआ, क्यों बैठ गए ?’’- पत्नी ने तेल की
कटोरी रखते हुए पूछा। बनारसी की माँ, वहाँ बच्चे थे, सो कुछ कह नहीं सका।
यहाँ एकान्त में तुमसे जरूरी बात करनी है।’’
‘‘क्या बात करनी है ?’’
‘‘बनारसी की ससुराल देखकर बड़ा दुःख हुआ। वे लोग बड़े गरीब हो गए हैं। दालान वगैरह तो टूट-फूट गया ही है, घर भी टूटा है। पता नहीं, बँटवारे के बाद इनके पास क्या बचा है। दामाद सायद हवेली की टंडैली करता है। कुछ भी समझ नहीं आता, क्या करूँ? ‘‘हाय राम ! क्यों करोगे ? बेटी का ब्याह हुआ है। ऐसी-वैसी बात न सोचो माता-पिता बेटी को जन्म देते हैं, करम तो ऊपर विधना लिखता है।’’
‘‘सीधे से सोचने पर हमें भी यही बात समझ में आती है। पर आँख से देखकर मक्खी निगली नहीं जाती। अब इधर पंचायत में हम लोगों के नियम किया है कि कोई हवेली में काम नहीं करेगा। वे लोग हवेली कमाने वाले लोग हैं, सो अलग।’’
‘‘तुम लोग आज ही नियम बनाए हो न ! जो पहले से हवेली पकड़कर बैठा है अचानक कैसे छोड़ दोगा ? समय दोगे न ! देखो जी, गरीब-अमीर हम नहीं जानते है। पाहुन का दिन पलटेगा जरूरी। घर बनाते कितनी देर लगती है ? गौना कराना है तो घर भी बनाएँगे।
‘‘तो तुम बेटी को उसी के घर भेजना चाहती हो?’’ ‘‘धर्म तो यही होता है।’’
‘‘धुत्त,. धर्म क्या कहेगा ? अपने यहाँ सात शादी होती है। कौन रोक है ? ’’
बिहार के ग्रामीण परिवेश पर लिखा गया नितांत अनूठा उपन्यास है, ‘फागुन के बाद’।
‘‘क्या बात करनी है ?’’
‘‘बनारसी की ससुराल देखकर बड़ा दुःख हुआ। वे लोग बड़े गरीब हो गए हैं। दालान वगैरह तो टूट-फूट गया ही है, घर भी टूटा है। पता नहीं, बँटवारे के बाद इनके पास क्या बचा है। दामाद सायद हवेली की टंडैली करता है। कुछ भी समझ नहीं आता, क्या करूँ? ‘‘हाय राम ! क्यों करोगे ? बेटी का ब्याह हुआ है। ऐसी-वैसी बात न सोचो माता-पिता बेटी को जन्म देते हैं, करम तो ऊपर विधना लिखता है।’’
‘‘सीधे से सोचने पर हमें भी यही बात समझ में आती है। पर आँख से देखकर मक्खी निगली नहीं जाती। अब इधर पंचायत में हम लोगों के नियम किया है कि कोई हवेली में काम नहीं करेगा। वे लोग हवेली कमाने वाले लोग हैं, सो अलग।’’
‘‘तुम लोग आज ही नियम बनाए हो न ! जो पहले से हवेली पकड़कर बैठा है अचानक कैसे छोड़ दोगा ? समय दोगे न ! देखो जी, गरीब-अमीर हम नहीं जानते है। पाहुन का दिन पलटेगा जरूरी। घर बनाते कितनी देर लगती है ? गौना कराना है तो घर भी बनाएँगे।
‘‘तो तुम बेटी को उसी के घर भेजना चाहती हो?’’ ‘‘धर्म तो यही होता है।’’
‘‘धुत्त,. धर्म क्या कहेगा ? अपने यहाँ सात शादी होती है। कौन रोक है ? ’’
बिहार के ग्रामीण परिवेश पर लिखा गया नितांत अनूठा उपन्यास है, ‘फागुन के बाद’।
लेखकीय
उपन्यास लिखने का गंभीर कार्य जो मैंने हाथ में लिया, उसका समापन हो गया।
ढेर सारी ऐसी ऊर्मियाँ हैं जिन्हें कहानी समेट नहीं पाती। ऐसे समय में
हमें उपन्यास लिखने की जरूरत महसूस होती है। लिखने का अलग-अलग कारण होता
होगा अलग-अलग लेखकों के लिए। मेरे लिए यह एक बड़ा कारण है कि मैं समाज से
बटोरे गए अनुभव विकास की धीमी प्रक्रिया से अधिक धीमी सरकने वाली शिक्षा
के कारण वंचित मानवता एवं अधकचरी अंध-व्यवस्था के फलस्वरूप स्वतंत्रता की
अर्थवत्ता खोने के आतंक के उबरने के लिए लिखती हूँ।
ढेर सारे क्षेत्र हैं काम करने को; परंतु मैंने लिखने को ही अलख जगाने का माध्यम चुना है। बिहार जैसी क्रांतिधर्मी मिट्टी में जनमी हूँ, जाति का वर्गीकरण मुझे कुलशीलयुक्त ब्राह्मण पुत्री, पुत्रवधू बना गया है, शिक्षा और समाज सुधार का लाभ मिला है। तिलयुगा नदी की मरणै धारा पर बना आश्रमनुमा घर, कौशिकी नदी की उत्फाल धारा से जूझती जिजीविषा सदानीरा बनी गंगा के किनारे विराम पाई मेरी लेखिका स्व को मिली है।
मेरा उपन्यास, ‘फागुन’ के बाद’ आजादी की आखिरी जंग से शुरू होकर सन् 56 तक पहुँचता है। 57 अर्थात् सन् 1957, 1857 का जश्न वर्ष था। तब तक लोग निराश नहीं हुए थे। भारत के स्वर्ग बनने की आशा बाकी थी, जनता अपनी सरकार पर विश्वास करती थी। सपने गिरनेवाले परदे की भाँति हौले-हौले सरकने लगे थे। परंतु उसकी रेशमी सरसराहट ने किसी को अब तक यह भान न होने दिया था कि वे छले जा रहे हैं, वंचित हो रहे हैं, उन्हें धोखा हो रहा है।
मैत्री तालाब के चारों ओर बसे उस छोटे से गाँव की करुणा यह थी कि 56 में ही चाँद बादलों में छिप गया है’ का एहसास हो गया था। उस छोटे से गाँव के माध्यम से मैंने यह बताने की छोटी-सी कोशिश की है कि हमें कब साकांक्ष हो जाना चाहिए था। मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ूँगी। मेरी लेखिका को अपने स्कूल की शिक्षिकाओं द्वारा कहा वाक्य सच बनाने का मन करता है-‘भारत गाँवों का देश है।’ हम पढ़े-लिखे लोग गाँव नगर की ओर बढ़ आए हैं। नगर हमें अपने आप में पूर्णतया लिप्त रखता है। तथापि हम गाँव से मुक्त नहीं होते। हमारा बिहार एक बड़ा-सा गाँव है, यहाँ अभी तक व्यक्ति का व्यक्ति से, जाति का जाति से परस्पर परिचय बना हुआ है।
प्रेम-घृणा हिंसा-अहिंसा दोस्ती-दुश्मनी चलती रहती है, परिचिति बनी रहती है। महानगरों में रहनेवाले भी इतने निर्लिप्त नहीं हैं, जो अपने गाँव को भूल पाए हैं। क्यों होता है ऐसा ? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे पशुधन के साथ हुआ, हमने गाँव तब बसाए जब स्थायी भोजन की व्यवस्था का ज्ञान हुआ। हमें गेहूँ, धान और दलहन का पता चला। हमें नमक के पहाड़ का भान हुआ, नमक का विकल्प नोनी का ज्ञान हुआ। हमें आज भी जंगल के शिकार की जरूरत पड़ती है, भोजन में; गेहूँ, चावल और दलहन की जरूरत पड़ती है। इस सामग्री को पॉलीथीन में बंद करें अथवा सेलेफिन कागज में; उपजाई जाती है गाँवों में। हमारा गाँव हमारे साथ है। हमारी संसदीय व्यवस्था में गाँव का आदमी सर्वोच्च कुरसियों पर विराजमान होता है और अपनी समस्याओं पर अनवरत बहसें करता रहता है, कमीशन बैठाता रहता है, अखबारों में छपाता रहता है। कृषि कार्य करने वाले सभी मजदूर शहरों को सजाने में लगे हैं, बिल्डिंगें बनाने में लगे हैं, सड़कों पर रोड़ियाँ और अलकतरे लुढ़काने में लगे हैं; पूरा-का पूरा गाँव नगरों के किनारे भद्दे और अस्वस्थ वातावरण में रहने को विवश है। विकास की लालसा में रोजी रोटी का स्थायी प्रबंध करने की ललक में पिसते ये सादे लोग छले जा रहे हैं।
ऐसे समय में मैं अपना सन् 56 तक का गाँव लेकर खड़ी हूँ। मेरे उपन्यास के सारे पात्र आपको संभवतः भारत के उन चारों वर्गों में किसी भी गाँव में मिल जाएँगे, जरा गरदन घुमाकर पीछे देखना होगा।
ढेर सारे क्षेत्र हैं काम करने को; परंतु मैंने लिखने को ही अलख जगाने का माध्यम चुना है। बिहार जैसी क्रांतिधर्मी मिट्टी में जनमी हूँ, जाति का वर्गीकरण मुझे कुलशीलयुक्त ब्राह्मण पुत्री, पुत्रवधू बना गया है, शिक्षा और समाज सुधार का लाभ मिला है। तिलयुगा नदी की मरणै धारा पर बना आश्रमनुमा घर, कौशिकी नदी की उत्फाल धारा से जूझती जिजीविषा सदानीरा बनी गंगा के किनारे विराम पाई मेरी लेखिका स्व को मिली है।
मेरा उपन्यास, ‘फागुन’ के बाद’ आजादी की आखिरी जंग से शुरू होकर सन् 56 तक पहुँचता है। 57 अर्थात् सन् 1957, 1857 का जश्न वर्ष था। तब तक लोग निराश नहीं हुए थे। भारत के स्वर्ग बनने की आशा बाकी थी, जनता अपनी सरकार पर विश्वास करती थी। सपने गिरनेवाले परदे की भाँति हौले-हौले सरकने लगे थे। परंतु उसकी रेशमी सरसराहट ने किसी को अब तक यह भान न होने दिया था कि वे छले जा रहे हैं, वंचित हो रहे हैं, उन्हें धोखा हो रहा है।
मैत्री तालाब के चारों ओर बसे उस छोटे से गाँव की करुणा यह थी कि 56 में ही चाँद बादलों में छिप गया है’ का एहसास हो गया था। उस छोटे से गाँव के माध्यम से मैंने यह बताने की छोटी-सी कोशिश की है कि हमें कब साकांक्ष हो जाना चाहिए था। मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ूँगी। मेरी लेखिका को अपने स्कूल की शिक्षिकाओं द्वारा कहा वाक्य सच बनाने का मन करता है-‘भारत गाँवों का देश है।’ हम पढ़े-लिखे लोग गाँव नगर की ओर बढ़ आए हैं। नगर हमें अपने आप में पूर्णतया लिप्त रखता है। तथापि हम गाँव से मुक्त नहीं होते। हमारा बिहार एक बड़ा-सा गाँव है, यहाँ अभी तक व्यक्ति का व्यक्ति से, जाति का जाति से परस्पर परिचय बना हुआ है।
प्रेम-घृणा हिंसा-अहिंसा दोस्ती-दुश्मनी चलती रहती है, परिचिति बनी रहती है। महानगरों में रहनेवाले भी इतने निर्लिप्त नहीं हैं, जो अपने गाँव को भूल पाए हैं। क्यों होता है ऐसा ? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे पशुधन के साथ हुआ, हमने गाँव तब बसाए जब स्थायी भोजन की व्यवस्था का ज्ञान हुआ। हमें गेहूँ, धान और दलहन का पता चला। हमें नमक के पहाड़ का भान हुआ, नमक का विकल्प नोनी का ज्ञान हुआ। हमें आज भी जंगल के शिकार की जरूरत पड़ती है, भोजन में; गेहूँ, चावल और दलहन की जरूरत पड़ती है। इस सामग्री को पॉलीथीन में बंद करें अथवा सेलेफिन कागज में; उपजाई जाती है गाँवों में। हमारा गाँव हमारे साथ है। हमारी संसदीय व्यवस्था में गाँव का आदमी सर्वोच्च कुरसियों पर विराजमान होता है और अपनी समस्याओं पर अनवरत बहसें करता रहता है, कमीशन बैठाता रहता है, अखबारों में छपाता रहता है। कृषि कार्य करने वाले सभी मजदूर शहरों को सजाने में लगे हैं, बिल्डिंगें बनाने में लगे हैं, सड़कों पर रोड़ियाँ और अलकतरे लुढ़काने में लगे हैं; पूरा-का पूरा गाँव नगरों के किनारे भद्दे और अस्वस्थ वातावरण में रहने को विवश है। विकास की लालसा में रोजी रोटी का स्थायी प्रबंध करने की ललक में पिसते ये सादे लोग छले जा रहे हैं।
ऐसे समय में मैं अपना सन् 56 तक का गाँव लेकर खड़ी हूँ। मेरे उपन्यास के सारे पात्र आपको संभवतः भारत के उन चारों वर्गों में किसी भी गाँव में मिल जाएँगे, जरा गरदन घुमाकर पीछे देखना होगा।
उषाकिरण खान
फागुन के बाद
फागुन के बाद का मौसम था, हवा में सूखापन आ गया था। पछुआ की तेज रफ्तार
अभी चलनी बाकी थी; पर यदा-कदा घूम जाती। आम के बौर लदे पेड़ अब टिकोरे
दिखाने लगे हैं। कोयल घमासान स्वर-युद्ध छेड़ बैठी थी। अगले साल मलमास
लगने वाला है, सो सूर्य-मास और चंद्र-मास का अंतर बढ़ गया है। संक्रांति
में देर है, उस लिहाज से अभी फागुन के चार दिन बच रहे हैं; जबकि होली हो
चुकी है। जितन मंडल के आँगन में बड़ी-सी गोल बखारी (अन्न रखने का पात्र)
लगभग चार कट्ठे भूमि के व्यास में खड़ी है। बखारी को धारण करनेवाले खूँटे
से बँधी बकरी-मुलुर मुलुर ताक रही है। उसके बच्चे यूँ ही उसकी टाँगों से
चिपके बैठे सोए हैं, अलसाए से। खूँटे के ऊपर लगे तख्ते का कुछ भाग चारों
ओर छूटा हुआ है; जिस पर कुछ लोग बैठे हैं, बेंचों की तरह। लंबूतरे आँगन
में कोने की ओर चूड़ा धमाधम कूटा जा रहा है।
घर की सबसे बड़ी बहू धान भूँज रही है, मँझली और छोटी उसे ओखल में डाल कूट रही हैं। सिर्फ मँझली बहू को ही चूड़ा कूटने की कला आती है। वही अच्छी तरह ठोकरा (बाँस की खपच्ची जिससे कूटते समय चूड़ा उकसाया जाता है) दे सकती है। बरामदे पर, आँगन में और चौपाल में ढेर सारे पुरुष बिखरे हैं। रामधनी जूट की रस्सी से सिकहर बना रहा है। रह-रहकर चोर नजरों से मँझली की ओर देख लेता है। छोटी नाटी सी मँझली का शरीर खूब सुडौल है आठ बच्चों को जनने के बाद भी नई नवेली लगती है। चूड़ा कूटते समय उठते-गिरते हाथ के साथ चंचल यौवन अब भी मंडल के हृदय को स्थिर नहीं रहने देता। ठोकरा देते हाथ के साथ संचालित नितंब उसे उतावला बनाने के लिए काफी हैं।
‘‘धुर मर्दे...’’कहकर अधबना सिकहर और पाट की लच्छियाँ ले रामधनी दालान की ओर चला।
‘‘कहाँ चले भाई, अच्छे तो थे यहीं। क्या हो गया ? बैठो, यहीं बैठो।’’
‘‘अरे जीजा, देखते नहीं, बहि पछाँहीवाली कैसे अंदोलन किए है !’’
जीजा जोर से हँसा। ‘‘तुम्हारी तो पुरानी आदत है। बाज नहीं आओगे। अरे तुम्हारे बेटे का कल ब्याह है। आज तुम मन भटकाते हो !’’
‘‘धुर सार, मन क्या अपने वश में है ? हम जानते हैं।’’
‘‘बैठो, इधर घूम जाओ...।’’
हँसी-खुसी का ऐसा ही वातावरण था। अगले मंगलवार को रामधनी के बेटे सुखीराम और भतीजे मनीराम का ब्याह होने वाला था। रामधनी का बेटा सात साल का था, भतीजा आठ साल का। कुशेश्वर स्थान के पासवाले गाँव बिजुआ में बारात जाएगी। रामधनी का बड़ा भाई झींगुर अपनी जाति का सरदार है, सो बारात सजी-बनी होनी चाहिए थी; पर एक खास कारण से यह बारात सजी-बनी नहीं होने वाली। यह तो सिर्फ अपने विशाल परिवार और निकट कुटुंबों की बारात होकर रहने वाली है। निकट कुटुंबों में भी सभी नहीं आने वाले हैं। कुछ सामाजिक अपमान के भय से मुँह छुपाए बैठे रहे। स्वयं रामधनी के मामा और ममेरे भाई नहीं आए हैं। इसके पीछे भी एक किस्सा है।
रामधनी जिस परिवार में अपना बेटा ब्याहने जा रहा है, उसका इतिहास भूगोल सामाजिक मान्यता को तरस रहा है। अगले मंगलवार को उसकी तरस पूरी हो जाएगी। अपनी जाति का सरदार अपना बेटा और भतीजा ब्याहने आ रहा है बारात लेकर। बात आज के संदर्भ में कोई बड़ी बात नहीं; पर उन दिनों के लिए बहुत बड़ी बात थी। नरपति मंडल की मौसी समस्तीपुर बाजार में मोदिआइन थी। बीच बाजार में उसकी दही-चिवड़ा पेड़ा और केला की दूकान थी। दूकान के पीछे उसकी पक्की हवेलीनुमा रिहाइश थी। कहते हैं, थोड़ी दूर हटकर गाँव में खेत-खलिहान भी था। काशीपुर के छन्नू बाबू की उसपर दयादृष्टि थी। छन्नू बाबू छोटे-मोटे जमींदार थे। मोदिआइन दूकान पर स्वयं बैठती थी। गोरे-चिट्टे रंगतवाली सुंदरी मोदिआइन मचिया पर पान खाती बैठी रहती। साफ पत्तल में बढ़िया दही-चिवड़ा ग्राहकों को खिलाती। चमचमाते साफ गिलास में पानी पीने को देती। अगल-बगल में ढेरसारी ऐसी दूकानें थीं; पर मोदिआइन की दूकान की दही लाजवाब होती। मोदिआइन की एक ही बेटी थी, उसे वह स्कूल पढ़ने भेजती।
नरपति मंडल भी कुछ दिन चोरी-चुपके अपनी मौसी के घर रहकर पढ़ता रहता था, फिर उसे गाँव में अपनी खेती सँभालने आना पड़ा। मोदिआइन की बेटी की शादी दूर युक्त प्रांत में किसी खाते-पीते सजातीय परिवार में छन्नू बाबू ने करवा दी थी। नरपति मंडल के ब्याह में मौसी ने बहू को साड़ी, कपड़ा और सोने के कर्णफूल भेजे थे। वह सब उन दिनों मंडल परिवार के लिए बड़ा कीमती था। वही मौसी मरने के पहले अपनी दूकान-जमीन सब नरपति के नाम कर गई थी। नरपति ने अंत समय में उसकी बड़ी सेवा की थी। कुछ तो सेवा से रीझकर, कुछ कोई और वारिस न होने की वजह से नरपति मंडल को यह हक मिला था। जाति बिरादरी में इसका बड़ा मजाक उड़ा था। परंतु नरपति मंडल ने जात की भात का अच्छा इंतजाम किया था और अपना पतिया छुड़ाकर फिर बछड़ों में शामिल हो गया था। सबकुछ होने के बाद भी वह अभी तक जातीय वक्रदृष्टि का शिकार था। उसकी चार बड़ी अर्थात् आठ, छः, चार और दो साल की बेटियाँ थीं। सद्यःजात एक बेटा भी था। कुछ तो उन दिनों छोटे बच्चों का विवाह विहित था, कुछ जाति में शामिल हो जाने की सबसे बड़ी कुंजी भी थी। जाति को भात के नाम पर जो विशाल भोज हुआ, जो पंचायत के लिए काँसे और पीतले के बरतन जुरमाने में दिए गए, उस खर्चे को भुनाना भी था। सरदार के घर बेटियों का विवाह कर नरपति मंडल ने अपना खोया सम्मान पा लिया।
सरदार सिर्फ सरदार नहीं था, उसका परिवार गाँव के सबसे बड़े ठाकुर का हसबखाह सिपाही था। औरतें हवेली कमाती थीं, मर्द मजदूरों के मेट थे। स्वयं सरदार ठाकुर साहब के साथ धोती गोलगंजी पहनकर दरभंगा कोर्ट-कचहरी जाता था। बड़े से आँगन में खपरैल घर था। दालान पर मचान बने थे। एक-आध तख्त भी थे। ठाकुर साहब के यहाँ से मिले खेत की पैदावर से आँगन की बखारी-कोठी भरे रहते थे। मौसी की संपत्ति से हुए संपन्न नरपति मंडल अपनी बेटी बनारसी और अजनास का विवाह प्रभावशाली संपन्न घर में कर, मूँछों पर ताव देने लगा था।
बारात क्या धज से निकली थी ! बारात के पहलेवाले दिन दोनों दूल्हे पीली धोती, कुरता और लाल गमछी में डोली में बैठ बिलौकी माँगने पहुँचे थे। आगे-आगे खुली डोली में काजल आँजे, जुल्फों से तेल चुआते दोनों दूल्हे, पीछे-पीछे गीत गाती औरतों की टोली-
घर की सबसे बड़ी बहू धान भूँज रही है, मँझली और छोटी उसे ओखल में डाल कूट रही हैं। सिर्फ मँझली बहू को ही चूड़ा कूटने की कला आती है। वही अच्छी तरह ठोकरा (बाँस की खपच्ची जिससे कूटते समय चूड़ा उकसाया जाता है) दे सकती है। बरामदे पर, आँगन में और चौपाल में ढेर सारे पुरुष बिखरे हैं। रामधनी जूट की रस्सी से सिकहर बना रहा है। रह-रहकर चोर नजरों से मँझली की ओर देख लेता है। छोटी नाटी सी मँझली का शरीर खूब सुडौल है आठ बच्चों को जनने के बाद भी नई नवेली लगती है। चूड़ा कूटते समय उठते-गिरते हाथ के साथ चंचल यौवन अब भी मंडल के हृदय को स्थिर नहीं रहने देता। ठोकरा देते हाथ के साथ संचालित नितंब उसे उतावला बनाने के लिए काफी हैं।
‘‘धुर मर्दे...’’कहकर अधबना सिकहर और पाट की लच्छियाँ ले रामधनी दालान की ओर चला।
‘‘कहाँ चले भाई, अच्छे तो थे यहीं। क्या हो गया ? बैठो, यहीं बैठो।’’
‘‘अरे जीजा, देखते नहीं, बहि पछाँहीवाली कैसे अंदोलन किए है !’’
जीजा जोर से हँसा। ‘‘तुम्हारी तो पुरानी आदत है। बाज नहीं आओगे। अरे तुम्हारे बेटे का कल ब्याह है। आज तुम मन भटकाते हो !’’
‘‘धुर सार, मन क्या अपने वश में है ? हम जानते हैं।’’
‘‘बैठो, इधर घूम जाओ...।’’
हँसी-खुसी का ऐसा ही वातावरण था। अगले मंगलवार को रामधनी के बेटे सुखीराम और भतीजे मनीराम का ब्याह होने वाला था। रामधनी का बेटा सात साल का था, भतीजा आठ साल का। कुशेश्वर स्थान के पासवाले गाँव बिजुआ में बारात जाएगी। रामधनी का बड़ा भाई झींगुर अपनी जाति का सरदार है, सो बारात सजी-बनी होनी चाहिए थी; पर एक खास कारण से यह बारात सजी-बनी नहीं होने वाली। यह तो सिर्फ अपने विशाल परिवार और निकट कुटुंबों की बारात होकर रहने वाली है। निकट कुटुंबों में भी सभी नहीं आने वाले हैं। कुछ सामाजिक अपमान के भय से मुँह छुपाए बैठे रहे। स्वयं रामधनी के मामा और ममेरे भाई नहीं आए हैं। इसके पीछे भी एक किस्सा है।
रामधनी जिस परिवार में अपना बेटा ब्याहने जा रहा है, उसका इतिहास भूगोल सामाजिक मान्यता को तरस रहा है। अगले मंगलवार को उसकी तरस पूरी हो जाएगी। अपनी जाति का सरदार अपना बेटा और भतीजा ब्याहने आ रहा है बारात लेकर। बात आज के संदर्भ में कोई बड़ी बात नहीं; पर उन दिनों के लिए बहुत बड़ी बात थी। नरपति मंडल की मौसी समस्तीपुर बाजार में मोदिआइन थी। बीच बाजार में उसकी दही-चिवड़ा पेड़ा और केला की दूकान थी। दूकान के पीछे उसकी पक्की हवेलीनुमा रिहाइश थी। कहते हैं, थोड़ी दूर हटकर गाँव में खेत-खलिहान भी था। काशीपुर के छन्नू बाबू की उसपर दयादृष्टि थी। छन्नू बाबू छोटे-मोटे जमींदार थे। मोदिआइन दूकान पर स्वयं बैठती थी। गोरे-चिट्टे रंगतवाली सुंदरी मोदिआइन मचिया पर पान खाती बैठी रहती। साफ पत्तल में बढ़िया दही-चिवड़ा ग्राहकों को खिलाती। चमचमाते साफ गिलास में पानी पीने को देती। अगल-बगल में ढेरसारी ऐसी दूकानें थीं; पर मोदिआइन की दूकान की दही लाजवाब होती। मोदिआइन की एक ही बेटी थी, उसे वह स्कूल पढ़ने भेजती।
नरपति मंडल भी कुछ दिन चोरी-चुपके अपनी मौसी के घर रहकर पढ़ता रहता था, फिर उसे गाँव में अपनी खेती सँभालने आना पड़ा। मोदिआइन की बेटी की शादी दूर युक्त प्रांत में किसी खाते-पीते सजातीय परिवार में छन्नू बाबू ने करवा दी थी। नरपति मंडल के ब्याह में मौसी ने बहू को साड़ी, कपड़ा और सोने के कर्णफूल भेजे थे। वह सब उन दिनों मंडल परिवार के लिए बड़ा कीमती था। वही मौसी मरने के पहले अपनी दूकान-जमीन सब नरपति के नाम कर गई थी। नरपति ने अंत समय में उसकी बड़ी सेवा की थी। कुछ तो सेवा से रीझकर, कुछ कोई और वारिस न होने की वजह से नरपति मंडल को यह हक मिला था। जाति बिरादरी में इसका बड़ा मजाक उड़ा था। परंतु नरपति मंडल ने जात की भात का अच्छा इंतजाम किया था और अपना पतिया छुड़ाकर फिर बछड़ों में शामिल हो गया था। सबकुछ होने के बाद भी वह अभी तक जातीय वक्रदृष्टि का शिकार था। उसकी चार बड़ी अर्थात् आठ, छः, चार और दो साल की बेटियाँ थीं। सद्यःजात एक बेटा भी था। कुछ तो उन दिनों छोटे बच्चों का विवाह विहित था, कुछ जाति में शामिल हो जाने की सबसे बड़ी कुंजी भी थी। जाति को भात के नाम पर जो विशाल भोज हुआ, जो पंचायत के लिए काँसे और पीतले के बरतन जुरमाने में दिए गए, उस खर्चे को भुनाना भी था। सरदार के घर बेटियों का विवाह कर नरपति मंडल ने अपना खोया सम्मान पा लिया।
सरदार सिर्फ सरदार नहीं था, उसका परिवार गाँव के सबसे बड़े ठाकुर का हसबखाह सिपाही था। औरतें हवेली कमाती थीं, मर्द मजदूरों के मेट थे। स्वयं सरदार ठाकुर साहब के साथ धोती गोलगंजी पहनकर दरभंगा कोर्ट-कचहरी जाता था। बड़े से आँगन में खपरैल घर था। दालान पर मचान बने थे। एक-आध तख्त भी थे। ठाकुर साहब के यहाँ से मिले खेत की पैदावर से आँगन की बखारी-कोठी भरे रहते थे। मौसी की संपत्ति से हुए संपन्न नरपति मंडल अपनी बेटी बनारसी और अजनास का विवाह प्रभावशाली संपन्न घर में कर, मूँछों पर ताव देने लगा था।
बारात क्या धज से निकली थी ! बारात के पहलेवाले दिन दोनों दूल्हे पीली धोती, कुरता और लाल गमछी में डोली में बैठ बिलौकी माँगने पहुँचे थे। आगे-आगे खुली डोली में काजल आँजे, जुल्फों से तेल चुआते दोनों दूल्हे, पीछे-पीछे गीत गाती औरतों की टोली-
कौने फुलवा फुलइ रामा आधि-आधि रतिया हय
कौने फुलवा फुलइ भिनसार हय।
आहो रामा, बेला फुलवा, फुलइ रामा आधि-आधि रतिया हय
चंपा फुलवा फुलइ भिनसार हय।
कौने फुलवा फुलइ भिनसार हय।
आहो रामा, बेला फुलवा, फुलइ रामा आधि-आधि रतिया हय
चंपा फुलवा फुलइ भिनसार हय।
सबसे पहले भीड़ बड़ी ठकुराइन की हवेली गई। बड़ी ठकुराइन चारों घरवासी सूर
भर-भरकर चावल बिलौकी के चंगेरे में डाल गईं। चवन्नी-अठन्नी सलामी भी मिली।
पूरा ठकुराहा घूमकर जब औरतें आँगन में पहुँचीं तब चावल से चंगेरे दौरे भर
गए थे; इकन्नी दूपैसाही और ताँबे के एक पैसे के सिक्कों से दोनों भावी
दूल्हों की जेबें भरी हुई थीं। सुखीराम घूमते-घूमते थककर चूर हो गया था।
वह अलसाकर डोली पर ही सो गया था। मनीराम को जोरों का जुकाम हो आया था, तो
पटापट छींक रहा था। बड़ी काकी अपने आँचल के खूँट से बार बार उसका मुँह
पोंछ दे रही थी। मन बहलाने को कह रही थी-‘यह छींक असगुन की
नहीं,
बच्चा सर्दी खा गया है, उसी की है।’
ठाकुर टोले से निकलते निकलते धूप में गरमी आ गई थी। मनीराम का सिर शायद पिराने लगा था। वह जोर जोर से रोने लगा। औरतें उन्हें लेकर आँगन में प्रवेश करने लगीं। डोली के आगे चलती औरतों ने झुंड बाँधकर एक तरह से राह रोक रखी थी और जोर-शोर से झूमर गाने लगी थीं-
ठाकुर टोले से निकलते निकलते धूप में गरमी आ गई थी। मनीराम का सिर शायद पिराने लगा था। वह जोर जोर से रोने लगा। औरतें उन्हें लेकर आँगन में प्रवेश करने लगीं। डोली के आगे चलती औरतों ने झुंड बाँधकर एक तरह से राह रोक रखी थी और जोर-शोर से झूमर गाने लगी थीं-
आगी आनय गेलहुँ ननदी के दुअरिया,
चकमक देवरेलाल, पियवा त’ गोयग नेने ठाढ़।
चकमक देवरेलाल, पियवा त’ गोयग नेने ठाढ़।
एक तरफ गीत का झमकता हुआ स्वर दूसरी ओर मनीराम का चीखना। अजीब समा था।
दालान पर से बुजुर्गवार उठकर हाँक लगा गए कि-‘बच्चे को उतारो रो
रहा
है।’
पर नक्कारखाने में तूती की आवाज सुनता ही कौन है ? शादी-ब्याह के घर का यही तो रमन-चमन है-रोना-गाना चीखना-चिल्लाना।
अवसर निकल ही आया। रामधनी ने देख लिया, पछाँहीवाली सेम की लतर उलट-पलटकर फलियाँ तोड़ रही थी। एकहाथ में सूप था, दूसरे से लतर पलट रही थी। ‘‘मैं कुछ मदद कर दूँ....?’’
लतर के ऐन सामने पतिको देख शरमा गई पछाँहीवाली, निष्फल प्रयास कर उठी अपने उत्तुंग यौवन को छुपाने का।
‘‘इस्स, कोई कहेगा, यह मेरी आठ बच्चों की माँ का शरीर है ! लगता है, कल ही गौना करा लाया।’’ पास आने को हुआ कि आँगन की ओर से आवाज आई-‘‘पछाँहीवाली, जितना हुआ उतना ही सेम ले आओ !’’-जिठानी चूल्हे के पास से हाँक लगा रही थी। अपनी लाल साड़ी सँभालती घूँघट आगे खींचती पछाँहीवाली सेमवाला सूप लिये आँगन की ओर भागी। रामधनी हँस पड़ा। अपनी बेफिक्र अदा में दालान की ओर निकल गया। उन दिनों इतनी खुराफात बहुत थी। पत्नी से मुलाकात कठिनाई से होती थी। इसलिए परिचित देहगंध का सतत आकर्षण बना रहता था।
सेम, आलू और बैंगन की रसेदार सब्जी तथा भात तैयार था। दालान पर मरद-मानुस नहा धोकर बालों में तेल डाल प्रस्तुत थे। खाना-पीना हुआ। दोनों दूल्हे राजा सजाए गए। दोनों के हाथों में कच्चे लोहे की छुरियाँ थीं, जिनमें साबुत सुपारी बँधी थीं। पैरों में आलता तथा गले में फूलों की माला थी। एक ही पालकी पर दोनों को सवार करना था। घर की देवी को प्रणाम करवा दादी ने उन्हें माँ के आँचल के नीचे दे दिया। माँएँ रोती-रोती बच्चों को अलग कर पालकी में बैठा आईं। जय गणेश, जय लुकेसरि कहकर पालकी उठाई गई। पालकी आँगन से गीतों के बीच निकली। बाराती भी चल पड़े। दूल्हों ने पहली बार अपनी माँओं को छोड़ा था, सो जोरों से रोने लगे। उधर बारात आँगन से निकली, इधर औरतों ने आँगन में तेल सिंदूर-बाँटना शुरू किया। तेल सिंदूर का खेल कुछ देर चलता रहा, फिर औरतें आराम करने लगीं। शाम ढलने में देर थी। रतजगा तो करना ही था। पहले क्यों न थोड़ा आराम कर लिया जाए, यह इरादा था। रात भर औरतें झूमर गाती नाचती रहीं। सुखीराम और मनीराम की माँ परेशान थीं। जब-जब बच्चों की सुधि आती, उनका दिल रोने को कर उठता। बच्चे भूखे होंगे, यह एहसास होता। सुखीराम तो अपनी माँ का कौर पोछन लड़का था, पर मनीराम की माँ फिर गर्भवती थी। संग सहेलियाँ हँसी-मजाक के बीच बोली भरोसा दे रही थीं।
‘‘ऐ भौजी बच्चों के लिए रोती हो ? अरे वे क्यों भूखे रहेंगे; समधी के यहां धेनु गाय है। उन्हीं का दूध पीकर मस्त होगा मेरा भतीजा।’’-छोटी ननद ने इठलाते हुए कहा था।
‘‘सुना है कि समधिन भी धेनु है। तगड़ी भी है। देवरजी और बहुआ दोनों रिपित कर देगी।’’
जिठानी ने इशारों ही में ऐसी मुद्रा बनाते हुए कहा कि रोती हुई माताएँ हँस पडीं। सुबह होते-होते थकी स्त्रियाँ सो गई थीं। आज का दिन पहाड़-सा बीतने वाला था। नरपति मंडल ने पहले ही कह रखा था कि वह बारात की मरजाद रखेगा। तीसरे दिन ही बिदाई हो सकेगी।
बिजुआ में आनंद बधावा बज रहा था। नरपति मंडल के ऊँचे डीह पर गहमागहमी थी। खपरैल दालान कुटुंबियों से भरे थे। बड़ा गोबर-लिपा आँगन नई रँगी लाल-पीली साड़ियोंवाली बेटी बहुओं से भरा था। चावल-दाल फटकती-बनती स्त्रियों के हाथों की चूड़ियों की खनक का मधुर स्वर वातावरण को उल्लास से भर रहा था। गूजावाला कटवी, पिटवी और जौसन बाजू आपस में टकराते तो मधुर स्वर बिखेरते यह स्वाभाविक ही था। इस विवाह में दूर-दूर के रिश्तेदार आए थे। समस्तीपुरवाली मोदिआइन की बेटी भी आने वाली थी, पर किसी कारणवश नहीं आ सकी। हाँ, मोदिआइन के ससुराल की दो स्त्रियाँ जरूर आई थीं। छींटदार नूरजहाँकट निमस्तीनवाला जंपर पहने वे औरतें अलग से पहचानी जाती थीं। बाकी औरतों ने नई काट का चुन्नटदार ब्लाउज पहन रखा था। समस्तीपुरवाली औरतों के जंपर में जेबें, थीं, जिनमें वे रोसड़ाबाजार की खास बीड़ी का बंडल और दिया सलाई की डिब्बी बड़ी सँभाल से रखतीं। गाँववाली औरतें हुक्का गुड़गुड़ातीं।
बड़ी-बड़ी परातों में भात तैयार कर रख दिया गया था। मिट्टी के बड़े-बड़े घड़ों में कढ़ी और बड़ी तैयार थे। दही और बुँदिया का भी इंतजाम था। नरपति मंडल ने दरवाजे पर हलवाई बैठाया था। बारातियों को बालूशाही और झिल्ली कचरी का नाश्ता करवाया गया था। पहले दिन बड़ा जब्बर खस्सी कटा था। दूसरे दिन बारातियों को मछली-भात का भोज दिया गया था। बारातियों के आगत-स्वागत के बीच दूल्हों पर किसी का ध्यान न गया। वैसे भी ऐसी शादियों में दूल्हे औरतों के हवाले कर दिए जाते थे। बेचारे बाल-दूल्हे गहमागहमी के बीच भौंचक से थे। औरतों के रात-भर के विधि-ब्यौहार ने उन्हें थका दिया था। वैसे विवाह आधे सोए आधेजगे में हुआ था। सुबह होने के बाद जब दोनों जोड़ियों की कोई विधि हो रही थी तभी उनमें लड़ाई छिड़ गई। हुआ यह कि खीर की थाली पर मनीराम झुक आया-गपागप खीर खाने लगा। सुखीराम उनींदा-सा चुपचाप देखता रहा। पर सुखीराम की सद्य:विवाहिता बनारसी ने मनीराम के आगे से थाली छीननी चाही। औरतें कौतुक से हँसने लगीं। मनीराम बनारसी के बाल पकड़कर खींचने लगा। बनारसी चीखकर रोने लगी। नींद में डूबा सुखीराम जग गया। वह मनीराम से अपनी दुलहन को बचाने के क्रम में उस पर चढ़ बैठा और लगा पिटाई करने। बड़ी बूढ़ियों ने बीच-बचाव किया तब जाकर लड़ाई थमी। अलग-अलग सबको खीर खाने को दी गई। विधि-ब्यौहार ताक पर गया। ऐसे बाल विवाहों में विधियों का ऐसा ही हस्र होता था। बहुत दिनों तक ये सब बातें मन बहलाव का कारण होती थीं।
जब सुखीराम ने घर आकर बड़ी अम्मा को यह बताया कि मनीराम मेरी कनियाँ के बाल नोचने लगा तब मनीराम ने भी कह दिया कि इसने भी वहाँ मेरी पिटाई कर दी। इस पर औरतों ने खासा मजा लिया। उन्होंने समझाया-
‘‘मनिया, तूने सुखिया की कनियाँ को कैसे छुआ ? वह तो तेरी भाबों होगी। अपने से छोटे भाई की औरत को नहीं छुआ जाता।’’
‘‘क्यों ? उसने क्यों मेरी थाली छीनी ?’’ मनीराम अब भी उस वंचित थाली की पीड़ा से मुक्त नहीं हुआ था।
‘‘फिर तो तुम्हें खीर मिली खाने को। मिली कि नहीं ?’’ सुखीराम ने कहा।
‘‘लेकिन तुमने मुझे मारा।’’
‘‘तुमने उसे क्यों मारा ?’’
‘‘हाँ-हाँ, ठीक ही तो कहता है सुखिया, तुमने उसकी कनियाँ को क्यों मारा ? यह भी कोई बात है ? अपनी कनियाँ को मारता।’’-मनीराम की अम्मा मुँह पर आँचल रख हँसती रही।
‘‘मेरी कनियाँ तो सोई थी वहीं पर चुपचाप। और यह भी तो सोया था। बुद्धू कहीं का !’’-इसी प्रकार की बातचीत देर तक रस ले लेकर होती रही थी। घर की औरतें खुश थीं कि डाला पर पूरी अठारह लाल-पीली तिनपढ़िया साड़ियाँ आई थीं। मर्द खुश थे कि बारात का स्वागत अच्छी तरह हुआ था तथा तीन सौ एक रुपयों की बिदाई हुई थी।
काफी दिनों तक औरतें मनीराम और सुखीराम को घेर-घेरकर पूछती रहीं कि किसकी कनियाँ ज्यादा सुंदर है। दोनों अपनी-अपनी कनियाँ को सुंदर बताते, यहाँ तक कि लड़ पड़ते। हाथापाई की नौबत आ जाती।
पछिया का जोर थमने लगा था। गेहूँ तैयार करके घर ले आया गया था। अगली खेती के लिए लोग खेत तैयार करने लग गए थे। सुखीराम और मनीराम काठ की पाटी लेकर पाठशाला जाने लगे थे। पाठशाला तो जाते, लेकिन ध्यान न रहने के कारण अकसर मास्टरजी से पिटते। धीरे-धीरे उनका जी उचट गया। तब तो फिर एक ही रास्ता बचा उनके लिए कि हवेली की टहलदारी करें। मनीराम अपनी माँ के साथ हवेली जाने लगा, सुखीराम ने भैंस चराने का काम अपने जिम्मे ले लिया।
उन्हीं दिनों गाँव में अचानक हैजे की महामारी फैली।
घर-के-घर साफ होने लगे। बड़ी हवेली की कन्यादानी बेटी जगदम्मा हैजे की भेंट चढ़ गई। उनका आँगन बड़ी हवेली से सटा पूरब की ओर था। तीन कोठरियों का एक खपरैल घर और ऊँचा बरामदा। जगदम्मा की उम्र उस समय मुश्किल से पचीस वर्ष रही होगी। कई मृत बच्चों को जन्म देने के बाद सबसे छोटा बेटा फेकू गोद में था। ईश्वर की लीला कि फेकू बच गया, जगदम्मा मर गई। सुखिया की माँ (धनीराम की औरत) की गोद में एक बच्ची थी, काली। उधर फेकू-दूध के लिए, अपनी माँ के लिए बेहाल होकर रोता। हवेली की बड़ी ठकुराइन ने रोते-रोते फेकू को सुखिया की माँ के आँचल में डाल दिया। ‘‘धनियाँ बो, इस अभागे फेकू की माँ बन जा। मेरी लाड़ली ननद का यह हाहुती बेटा जी जाए। तुझे कोई कमी न रहने दूँगी। तेरा खाना पीना यहीं होगा। चितकबरी गाय का साँझ का दूँध तू पीना। इसे छाती से लगा ले।’’-धनियाँ बो ने तुरंत फेकू बाबू को आँचल से ढाँप लिया। बच्चा भूखा था, मिनटों में दूध पीकर सो गया। अब धनीराम की औरत फेकू बाबू की अम्मा थी। घर में कोई उसे भारी काम न करने देता। सब उसके खाने-पीने का ख्याल रखते। हवेली में भी यही होता है। पर धनीराम की औरत पतराखन थी। दो बच्चों को दूध पिलाती सारा काम करती रहती शिशु फेकू मुश्किल से पंद्रह दिनों तक अपनी माँ को खोजता रहा, फिर भूल गया।
पर नक्कारखाने में तूती की आवाज सुनता ही कौन है ? शादी-ब्याह के घर का यही तो रमन-चमन है-रोना-गाना चीखना-चिल्लाना।
अवसर निकल ही आया। रामधनी ने देख लिया, पछाँहीवाली सेम की लतर उलट-पलटकर फलियाँ तोड़ रही थी। एकहाथ में सूप था, दूसरे से लतर पलट रही थी। ‘‘मैं कुछ मदद कर दूँ....?’’
लतर के ऐन सामने पतिको देख शरमा गई पछाँहीवाली, निष्फल प्रयास कर उठी अपने उत्तुंग यौवन को छुपाने का।
‘‘इस्स, कोई कहेगा, यह मेरी आठ बच्चों की माँ का शरीर है ! लगता है, कल ही गौना करा लाया।’’ पास आने को हुआ कि आँगन की ओर से आवाज आई-‘‘पछाँहीवाली, जितना हुआ उतना ही सेम ले आओ !’’-जिठानी चूल्हे के पास से हाँक लगा रही थी। अपनी लाल साड़ी सँभालती घूँघट आगे खींचती पछाँहीवाली सेमवाला सूप लिये आँगन की ओर भागी। रामधनी हँस पड़ा। अपनी बेफिक्र अदा में दालान की ओर निकल गया। उन दिनों इतनी खुराफात बहुत थी। पत्नी से मुलाकात कठिनाई से होती थी। इसलिए परिचित देहगंध का सतत आकर्षण बना रहता था।
सेम, आलू और बैंगन की रसेदार सब्जी तथा भात तैयार था। दालान पर मरद-मानुस नहा धोकर बालों में तेल डाल प्रस्तुत थे। खाना-पीना हुआ। दोनों दूल्हे राजा सजाए गए। दोनों के हाथों में कच्चे लोहे की छुरियाँ थीं, जिनमें साबुत सुपारी बँधी थीं। पैरों में आलता तथा गले में फूलों की माला थी। एक ही पालकी पर दोनों को सवार करना था। घर की देवी को प्रणाम करवा दादी ने उन्हें माँ के आँचल के नीचे दे दिया। माँएँ रोती-रोती बच्चों को अलग कर पालकी में बैठा आईं। जय गणेश, जय लुकेसरि कहकर पालकी उठाई गई। पालकी आँगन से गीतों के बीच निकली। बाराती भी चल पड़े। दूल्हों ने पहली बार अपनी माँओं को छोड़ा था, सो जोरों से रोने लगे। उधर बारात आँगन से निकली, इधर औरतों ने आँगन में तेल सिंदूर-बाँटना शुरू किया। तेल सिंदूर का खेल कुछ देर चलता रहा, फिर औरतें आराम करने लगीं। शाम ढलने में देर थी। रतजगा तो करना ही था। पहले क्यों न थोड़ा आराम कर लिया जाए, यह इरादा था। रात भर औरतें झूमर गाती नाचती रहीं। सुखीराम और मनीराम की माँ परेशान थीं। जब-जब बच्चों की सुधि आती, उनका दिल रोने को कर उठता। बच्चे भूखे होंगे, यह एहसास होता। सुखीराम तो अपनी माँ का कौर पोछन लड़का था, पर मनीराम की माँ फिर गर्भवती थी। संग सहेलियाँ हँसी-मजाक के बीच बोली भरोसा दे रही थीं।
‘‘ऐ भौजी बच्चों के लिए रोती हो ? अरे वे क्यों भूखे रहेंगे; समधी के यहां धेनु गाय है। उन्हीं का दूध पीकर मस्त होगा मेरा भतीजा।’’-छोटी ननद ने इठलाते हुए कहा था।
‘‘सुना है कि समधिन भी धेनु है। तगड़ी भी है। देवरजी और बहुआ दोनों रिपित कर देगी।’’
जिठानी ने इशारों ही में ऐसी मुद्रा बनाते हुए कहा कि रोती हुई माताएँ हँस पडीं। सुबह होते-होते थकी स्त्रियाँ सो गई थीं। आज का दिन पहाड़-सा बीतने वाला था। नरपति मंडल ने पहले ही कह रखा था कि वह बारात की मरजाद रखेगा। तीसरे दिन ही बिदाई हो सकेगी।
बिजुआ में आनंद बधावा बज रहा था। नरपति मंडल के ऊँचे डीह पर गहमागहमी थी। खपरैल दालान कुटुंबियों से भरे थे। बड़ा गोबर-लिपा आँगन नई रँगी लाल-पीली साड़ियोंवाली बेटी बहुओं से भरा था। चावल-दाल फटकती-बनती स्त्रियों के हाथों की चूड़ियों की खनक का मधुर स्वर वातावरण को उल्लास से भर रहा था। गूजावाला कटवी, पिटवी और जौसन बाजू आपस में टकराते तो मधुर स्वर बिखेरते यह स्वाभाविक ही था। इस विवाह में दूर-दूर के रिश्तेदार आए थे। समस्तीपुरवाली मोदिआइन की बेटी भी आने वाली थी, पर किसी कारणवश नहीं आ सकी। हाँ, मोदिआइन के ससुराल की दो स्त्रियाँ जरूर आई थीं। छींटदार नूरजहाँकट निमस्तीनवाला जंपर पहने वे औरतें अलग से पहचानी जाती थीं। बाकी औरतों ने नई काट का चुन्नटदार ब्लाउज पहन रखा था। समस्तीपुरवाली औरतों के जंपर में जेबें, थीं, जिनमें वे रोसड़ाबाजार की खास बीड़ी का बंडल और दिया सलाई की डिब्बी बड़ी सँभाल से रखतीं। गाँववाली औरतें हुक्का गुड़गुड़ातीं।
बड़ी-बड़ी परातों में भात तैयार कर रख दिया गया था। मिट्टी के बड़े-बड़े घड़ों में कढ़ी और बड़ी तैयार थे। दही और बुँदिया का भी इंतजाम था। नरपति मंडल ने दरवाजे पर हलवाई बैठाया था। बारातियों को बालूशाही और झिल्ली कचरी का नाश्ता करवाया गया था। पहले दिन बड़ा जब्बर खस्सी कटा था। दूसरे दिन बारातियों को मछली-भात का भोज दिया गया था। बारातियों के आगत-स्वागत के बीच दूल्हों पर किसी का ध्यान न गया। वैसे भी ऐसी शादियों में दूल्हे औरतों के हवाले कर दिए जाते थे। बेचारे बाल-दूल्हे गहमागहमी के बीच भौंचक से थे। औरतों के रात-भर के विधि-ब्यौहार ने उन्हें थका दिया था। वैसे विवाह आधे सोए आधेजगे में हुआ था। सुबह होने के बाद जब दोनों जोड़ियों की कोई विधि हो रही थी तभी उनमें लड़ाई छिड़ गई। हुआ यह कि खीर की थाली पर मनीराम झुक आया-गपागप खीर खाने लगा। सुखीराम उनींदा-सा चुपचाप देखता रहा। पर सुखीराम की सद्य:विवाहिता बनारसी ने मनीराम के आगे से थाली छीननी चाही। औरतें कौतुक से हँसने लगीं। मनीराम बनारसी के बाल पकड़कर खींचने लगा। बनारसी चीखकर रोने लगी। नींद में डूबा सुखीराम जग गया। वह मनीराम से अपनी दुलहन को बचाने के क्रम में उस पर चढ़ बैठा और लगा पिटाई करने। बड़ी बूढ़ियों ने बीच-बचाव किया तब जाकर लड़ाई थमी। अलग-अलग सबको खीर खाने को दी गई। विधि-ब्यौहार ताक पर गया। ऐसे बाल विवाहों में विधियों का ऐसा ही हस्र होता था। बहुत दिनों तक ये सब बातें मन बहलाव का कारण होती थीं।
जब सुखीराम ने घर आकर बड़ी अम्मा को यह बताया कि मनीराम मेरी कनियाँ के बाल नोचने लगा तब मनीराम ने भी कह दिया कि इसने भी वहाँ मेरी पिटाई कर दी। इस पर औरतों ने खासा मजा लिया। उन्होंने समझाया-
‘‘मनिया, तूने सुखिया की कनियाँ को कैसे छुआ ? वह तो तेरी भाबों होगी। अपने से छोटे भाई की औरत को नहीं छुआ जाता।’’
‘‘क्यों ? उसने क्यों मेरी थाली छीनी ?’’ मनीराम अब भी उस वंचित थाली की पीड़ा से मुक्त नहीं हुआ था।
‘‘फिर तो तुम्हें खीर मिली खाने को। मिली कि नहीं ?’’ सुखीराम ने कहा।
‘‘लेकिन तुमने मुझे मारा।’’
‘‘तुमने उसे क्यों मारा ?’’
‘‘हाँ-हाँ, ठीक ही तो कहता है सुखिया, तुमने उसकी कनियाँ को क्यों मारा ? यह भी कोई बात है ? अपनी कनियाँ को मारता।’’-मनीराम की अम्मा मुँह पर आँचल रख हँसती रही।
‘‘मेरी कनियाँ तो सोई थी वहीं पर चुपचाप। और यह भी तो सोया था। बुद्धू कहीं का !’’-इसी प्रकार की बातचीत देर तक रस ले लेकर होती रही थी। घर की औरतें खुश थीं कि डाला पर पूरी अठारह लाल-पीली तिनपढ़िया साड़ियाँ आई थीं। मर्द खुश थे कि बारात का स्वागत अच्छी तरह हुआ था तथा तीन सौ एक रुपयों की बिदाई हुई थी।
काफी दिनों तक औरतें मनीराम और सुखीराम को घेर-घेरकर पूछती रहीं कि किसकी कनियाँ ज्यादा सुंदर है। दोनों अपनी-अपनी कनियाँ को सुंदर बताते, यहाँ तक कि लड़ पड़ते। हाथापाई की नौबत आ जाती।
पछिया का जोर थमने लगा था। गेहूँ तैयार करके घर ले आया गया था। अगली खेती के लिए लोग खेत तैयार करने लग गए थे। सुखीराम और मनीराम काठ की पाटी लेकर पाठशाला जाने लगे थे। पाठशाला तो जाते, लेकिन ध्यान न रहने के कारण अकसर मास्टरजी से पिटते। धीरे-धीरे उनका जी उचट गया। तब तो फिर एक ही रास्ता बचा उनके लिए कि हवेली की टहलदारी करें। मनीराम अपनी माँ के साथ हवेली जाने लगा, सुखीराम ने भैंस चराने का काम अपने जिम्मे ले लिया।
उन्हीं दिनों गाँव में अचानक हैजे की महामारी फैली।
घर-के-घर साफ होने लगे। बड़ी हवेली की कन्यादानी बेटी जगदम्मा हैजे की भेंट चढ़ गई। उनका आँगन बड़ी हवेली से सटा पूरब की ओर था। तीन कोठरियों का एक खपरैल घर और ऊँचा बरामदा। जगदम्मा की उम्र उस समय मुश्किल से पचीस वर्ष रही होगी। कई मृत बच्चों को जन्म देने के बाद सबसे छोटा बेटा फेकू गोद में था। ईश्वर की लीला कि फेकू बच गया, जगदम्मा मर गई। सुखिया की माँ (धनीराम की औरत) की गोद में एक बच्ची थी, काली। उधर फेकू-दूध के लिए, अपनी माँ के लिए बेहाल होकर रोता। हवेली की बड़ी ठकुराइन ने रोते-रोते फेकू को सुखिया की माँ के आँचल में डाल दिया। ‘‘धनियाँ बो, इस अभागे फेकू की माँ बन जा। मेरी लाड़ली ननद का यह हाहुती बेटा जी जाए। तुझे कोई कमी न रहने दूँगी। तेरा खाना पीना यहीं होगा। चितकबरी गाय का साँझ का दूँध तू पीना। इसे छाती से लगा ले।’’-धनियाँ बो ने तुरंत फेकू बाबू को आँचल से ढाँप लिया। बच्चा भूखा था, मिनटों में दूध पीकर सो गया। अब धनीराम की औरत फेकू बाबू की अम्मा थी। घर में कोई उसे भारी काम न करने देता। सब उसके खाने-पीने का ख्याल रखते। हवेली में भी यही होता है। पर धनीराम की औरत पतराखन थी। दो बच्चों को दूध पिलाती सारा काम करती रहती शिशु फेकू मुश्किल से पंद्रह दिनों तक अपनी माँ को खोजता रहा, फिर भूल गया।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book